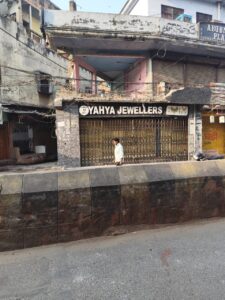भारतीय बैंकिंग तंत्र में इस समय नकदी की कोई कमी नहीं है। आँकड़े बताते हैं कि बैंकों के पास जून तक ₹3–4 ट्रिलियन की अतिरिक्त लिक्विडिटी मौजूद है। इसके बावजूद, कर्ज़ वितरण की रफ्तार तेज़ होने के बजाय धीमी बनी हुई है। सवाल उठता है कि जब संसाधन पर्याप्त हैं, तो बैंक उद्यमों, कारोबारियों और सामान्य ग्राहकों को ऋण देने से क्यों झिझक रहे हैं?
क्या कारण हैं इस झिझक के?
1️⃣ जोखिम का डर:
बैंक पिछले वर्षों में हुए बड़े NPA (non-performing assets) संकट से उबर तो गए हैं, लेकिन पुरानी चोट का डर अभी भी गहरा है। खासकर उन सेक्टरों को लेकर, जहाँ पहले डूबत खातों की संख्या ज़्यादा रही।
2️⃣ बदलते आर्थिक हालात:
वैश्विक स्तर पर ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव, भू-राजनीतिक तनाव, और घरेलू महँगाई के कारण निवेश के फैसलों में भी सतर्कता बढ़ी है। इससे लोन की मांग भी कम हुई है, और बैंक भी संभलकर कदम रख रहे हैं।
3️⃣ प्रक्रियात्मक सख्ती:
ऋण मंज़ूरी की प्रक्रियाएँ और शर्तें कड़ी हुई हैं, जिससे छोटे और मझोले उद्योगों (MSME) को लोन पाना कठिन हो गया है। कई बार ज़रूरतमंद को कर्ज़ की शर्तें समझ ही नहीं आतीं या वे कागज़ी औपचारिकताओं में उलझ जाते हैं।
इसका असर कहाँ दिखता है?
- छोटे उद्योगों की विकास दर धीमी होती है।
- रोज़गार के नए अवसर कम बनते हैं।
- खपत और निवेश की गति भी थम जाती है, जिससे आर्थिक चक्र सुस्त पड़ता है।
क्या हो सकते हैं समाधान?
- बैंकों को अपने जोखिम मूल्यांकन मॉडल में सुधार कर, ज़मीनी स्तर पर व्यवसायों और स्टार्टअप्स को समझना होगा।
- MSME और नई परियोजनाओं के लिए खास ऋण योजनाएँ और लचीलापन ज़रूरी है।
- सरकार और नियामक संस्थाओं को नीतियों में ऐसी सरलता लानी चाहिए कि सशक्त निगरानी बनी रहे, मगर निवेशकों और उद्यमियों को भरोसा भी मिले।
आज ज़रूरत सिर्फ संसाधन जुटाने की नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा में लगाने की है। बैंकिंग व्यवस्था में नकदी का बहाव तभी सार्थक होगा, जब वह उद्योग, रोज़गार और नवाचार तक पहुँचे। भारत की तेज़ रफ़्तार अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए बैंकों को अपनी झिझक छोड़कर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा — समझदारी और संतुलन के साथ।